भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं....
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥
(गीता ६/३५)
हे महाबाहु कुन्तीपुत्र! इसमे कोई संशय नही है कि चंचल मन को वश में करना अत्यन्त कठिन है, किन्तु इसे सभी सांसारिक कामनाओं के त्याग (वैराग्य) और निरन्तर अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है।
भगवान ने हमें समस्त भौतिक कर्मों को करने के लिये तीन वस्तु दी हैं, (१) बुद्धि, (२) मन और (३) इन्द्रियों का समूह यह शरीर। बुद्धि के द्वारा हमें जानना होता है, मन के द्वारा हमें मानना होता है और इन्द्रियों के द्वारा हमें करना होता है।
इसके लिये पहले इच्छा और कामना का भेद समझना होगा, कामनाओं का जन्म बुद्धि के द्वारा होता है, और इच्छाओं का जन्म मन में होता है। बुद्धि का वास स्थान मष्तिष्क होता है और मन का वास स्थान हृदय होता है, बुद्धि विषयों की ओर आकर्षित होकर कामनाओं को उत्पन्न करती हैं और इच्छायें प्रारब्ध के कारण मन में उत्पन्न होती हैं। कामना जीवन में कभी पूर्ण नहीं होती है, इच्छा हमेशा पूर्ण होती हैं।
बुद्धि के अन्दर विवेक होता है, यह विवेक केवल मनुष्यों में ही होता है, अन्य किसी योनि में नहीं होता है। यह विवेक हंस के समान होता है। इस विवेक रूपी हंस के द्वारा "जल मिश्रित दूध" के समान "शरीर मिश्रित आत्मा" में से जल रूपी शरीर और दूध रूपी आत्मा का अलग-अलग अनुभव किया जाता है, जो जीव आत्मा और शरीर का अलग-अलग अनुभव कर लेता है तो वह जीव केवल दूध रूपी आत्मा का ही रस पान करके तृप्त हो जाता है और शरीर रूपी जल की आसक्ति का त्याग करके वह निरन्तर आत्मा में ही स्थित होकर परम आनन्द का अनुभव करता है।
मनुष्य शरीर रथ के समान है, इस रथ में घोडे रूपी इन्द्रियाँ हैं, लगाम रूपी मन है, सारथी रूपी बुद्धि है और रथ के दो स्वामी जीव कर्ता-भाव में अहंकार से ग्रसित रहता है और आत्मा द्रृष्टा-भाव में मुक्त रहता है। जब तक जीव का विवेक सुप्त अवस्था में रहता है तब तक जीव स्वयं को कर्ता समझकर शरीर रूपी रथ के इन्द्रियों रूपी घोड़ो को मन रूपी लगाम से बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा चलाता रहता है, तो जीव कर्म के बंधन में फंसकर कर्म के अनुसार सुख-दुख भोगता रहता है।
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
जब जीव का विवेक भगवान की कृपा से सत्संग के द्वारा जाग्रत होता है तब जीव मन रुपी लगाम को बुद्धि रुपी सारथी सहित आत्मा को सोंप देता है तब जीव अकर्ता भाव में द्रृष्टा-भाव में स्थित होकर मुक्त हो जाता है।
जब तक जीव के शरीर रूपी रथ का बुद्धि रूपी सारथी मन रुपी लगाम को खींचकर नही रखता है तो इन्द्रियाँ रुपी घोंडे अनियन्त्रित रूप से विषयों की ओर आकर्षित होकर शरीर रुपी इस रथ को दौड़ाते ही रहते हैं, और अधिक दौड़ने के कारण शरीर रुपी रथ शीघ्र थककर चलने की स्थिति में नही रह जाता है फिर एक दिन काल के रूप में एक हवा का झोंका आता है और जीव को पुराने रथ से उड़ाकर नये रथ पर ले जाता है।
आत्मा ही जीव का परम मित्र है, वह जीव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, वही जीव का वास्तविक हितैशी है, इसलिये वह भी जीव के साथ नये रथ पर चला जाता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक जीव स्वभाव द्वारा बुद्धि सहित मन को आत्मा को नहीं सोंप देता है।
मन चंचल कभी नहीं होता है, बुद्धि चंचल होती है, बुद्धि की चंचलता के कारण ही मन चंचल प्रतीत होता है। क्योंकि मन बुद्धि के वश में होता है बुद्धि मन को अपने अनुसार चलाती है तो बुद्धि की आज्ञा मान कर मन उधर की ओर चल देता है, हम समझतें हैं मन चंचल है।
जिस प्रकार कोई कोई पति अपनी पत्नी के पूर्ण आधीन होता है तो वह जोरु का गुलाम कहलाता हैं, और जब पत्नी अपने पति के पूर्ण आधीन रहती है तो वह पतिव्रता स्त्री कहलाती है, ठीक उसी प्रकार बुद्धि पत्नी (स्त्रीलिंग) स्वरूपा है और मन (पुल्लिंग) पति स्वरूप है, जब मन, बुद्धि के आधीन होता है तो वह जोरु के गुलाम की तरह नाचता रहता है, और जब बुद्धि स्वयं मन के आधीन हो जाती है तो वह स्थिर हो जाती है तो मन भी स्थिर हो जाता है।
मनुष्य को अपने मन रूपी दूध का बुद्धि की मथानी बनाकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि असुरों और धैर्य, क्षमा, सरलता, संकल्प, सत्य आदि देवताओं द्वारा अहंकार की डोरी से मथकर भाव रूपी मक्खन का भोग प्रभु को लगाना चाहिये। यही माखन मेरे कृष्णा को अत्यन्त पसन्द है। जो छाछ बचेगी वह मेरा कान्हा आपसे स्वयं माँग कर खुद ही पी लेगा, मन रूपी दूध का कोई भी अंश नहीं शेष नहीं रहता है। यही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है।
॥ हरि ॐ तत् सत् ॥
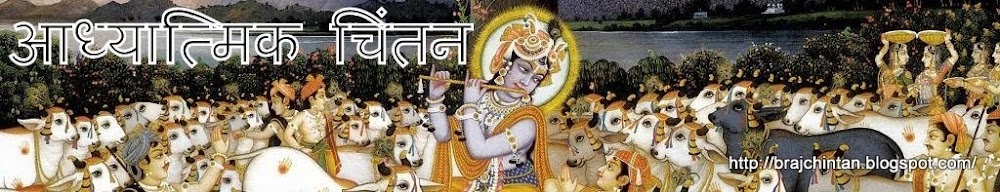
.jpg)