भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं....
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥
(गीताः १२/२)
जो मनुष्य मुझमें अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण-साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं, और अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं वह मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। १. जिस विधि से भक्ति वृद्धि को प्राप्त होती है, उस विधि का निरूपण किया जाता है, सांसारिक आसक्ति के त्याग से, कृष्ण कथा सुनने से और कृष्ण नाम के कीर्तन से ही भक्ति रूपी बीज दृढ़ स्थित होता है।
२. घर में रहकर ही अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए ही भक्ति का बीज दृढ़ होता है, सांसारिक इच्छाओं को सीमित कर मन को स्थिर करके मूर्ति पूजा के द्वारा, कथा श्रवण आदि विधियों से भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिये।
३. सांसारिक इच्छाओं के होते हुए भी चित्त को श्रीहरि के श्रवण आदि में प्रयत्न करके निरन्तर लगाये रखना चाहिए, और तब तक लगाये रखना चाहिये जब तक भगवान से प्रेम तथा आसक्ति और राग उत्पन्न न हो जाये।
४. शास्त्रों के अनुसार भक्ति के बीज को तभी दृढ़ स्थित कहा जा सकता है जब-तक अन्य किसी के प्रति प्रेम और आसक्ति नहीं रह जाती है और घर के प्रति स्वत: ही आसक्ति का अन्त नहीं हो जाता है।
५. जब घर एक बाधक और शरीर, आत्मा से अलग लगने लगता है, केवल श्रीकृष्ण की भक्ति ही एकमात्र कर्म हो जाता है, तभी प्राणी कृतार्थ हो पाता है।
६. कर्तव्य पूर्ण हो जाने पर या भक्ति के प्राप्त होने पर भी सदैव घर में निवास करने से भक्ति का विनाश हो जाता है, इसलिए घर का त्याग करके मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिये।
७. इस प्रकार निरन्तर प्रयत्न करने से सम्पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति में स्थिरता प्राप्त हो जाती है, घर त्याग करने में दुष्ट लोगों की संगति और भोजन प्रमुख बाधाएँ होती हैं।
८. इसलिए भगवान के मंदिर के समीप तथा भक्तों के साथ निवास करना चाहिये, भक्तों के पास रहें या भक्तों से दूर रहें लेकिन इस प्रकार रहना चाहिये जिससे मन दूषित न हो सके।
९. भगवान की सेवा करने से या भगवान की कथा श्रवण करने से जिस प्रकार से भी भगवान के प्रति आसक्ति दृड़ हो सके, इस प्रकार जीवन की अन्तिम श्वांस तक सेवा या श्रवण करते रहना चाहिए।
१०. किसी बाधा की संभावना से या हठपूर्वक एकान्त में रहने की इच्छा नहीं करनी चाहिये बल्कि भय मुक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक एकान्त में रहना चाहिये, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से सभी प्रकार से रक्षा करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिये।
११. इस प्रकार भगवत प्राप्ति की इच्छा वालों के लिये शास्त्रों के गूढ़ तत्त्व का निरूपण किया गया है, जो भी इस विधि का दृड़ता-पूर्वक पालन करता है, वह भगवान में दृढ़ स्थिति को प्राप्त ही जाता है।
१२. इस प्रकार भगवान प्राप्ति की इच्छा वालों के लिये शास्त्रों के रहस्यमय तत्त्व का निरूपण किया गया है, जो भी इस विधि का स्थिरता के साथ पालन करता है, वह भगवान में स्थिर स्थिति को प्राप्त हो ही जाता है।
॥ हरि ॐ तत् सत् ॥
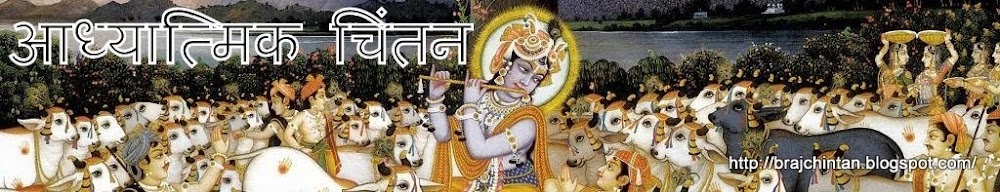
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)