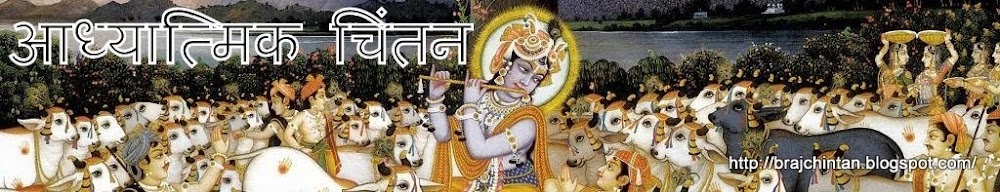भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं....
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥
(गीताः २/१३)
जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था को निरन्तर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है, ऎसे परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥
(गीताः २/१३)
बात त्रेतायुग की है, अष्टावक्र नामक एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे, उनका शरीर आठ भागों में टेढ़ा था, जब वह चलते थे तो साधारण लोग उन्हे देखकर हँसते थे, लेकिन वह हृदय से अत्यन्त पवित्र थे, क्योंकि उन्होने अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया था, वह शरीर और आत्मा का भेद जानते थे।
एक बार महाराज जनक ने ऋषियों की सभा का आयोजन किया, उस सभा में अष्टावक्र ऋषि को भी आमन्त्रित किया, जैसे ही ऋषि ने सभा में प्रवेश किया वहाँ पर उपस्थित सभी सदस्य उनको देखकर हँसने लगे तो उन सभी को हँसते हुए देखकर ऋषि अष्टावक्र भी जोर-जोर से हँसने लगे, सभी सदस्य एक दूसरे से कहने लगे हम सभी उनको देखकर हँस रहे हैं परन्तु वह तो हमसे भी जोर से हँस रहें है, "इसका क्या कारण है?"
यह सब देखकर राजा जनक ने सिंहासन से उठकर नम्रता-पूर्वक ऋषि अष्टावक्र से पूछा, "हे ऋषि आप किस कारण इतनी जोर से हँस रहे है?"
ऋषि अष्टावक्र ने कहा, "मैं सोच रहा था कि मैं ऋषियों-मुनियों की सभा में आया हूँ, परन्तु मैं तो चमड़े के व्यापारी मोचियों की सभा में पहुँच गया हूँ, एक मोची की दृष्टि केवल चमड़े में होती है, अत: मैं देख रहा हूँ कि आप सभी की दृष्टि मेरी नश्वर चमड़ी पर ही है, इसलिये आप मेरी नित्य-आत्मा का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं।
आत्मा की उपेक्षा करके बाहरी नश्वर शरीर को महत्व देना अज्ञान है।
ऋषि अष्टावक्र के शब्दों को सुनकर राजा जनक के हृदय में अत्यन्त पश्चाताप हुआ, वह समझ गये कि ऋषि एक आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, यही सिंहासन पर बैठाने योग्य हैं, तब राजा जनक ने भाव-विभोर होकर बड़ॆ आदर के साथ सिंहासन पर बैठाकर उन्हे साष्टांग प्रणाम किया और सद्गुरु रूप में स्वीकार किया।
शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, यह भौतिक शरीर तो हड्डी, खून, माँस का एक घड़ा मात्र है, मन और बुद्धि भी इस शरीर के अंग ही हैं, परन्तु आत्मा इन सबसे अलग है, बुद्धि इस अनित्य संसार को ही सत्य समझती है और मन इन अस्थायी सांसारिक भावों को ही वास्तविक मानता है, जिसके कारण यह क्षणिंक सुख की अनुभूति ही अत्यधिक दुख का कारण बनती है, हम सभी इस शरीर, मन और बुद्धि से अलग आत्मा हैं।
हमारा यह शरीर तो एक पिंजरे के समान जिसमें जीवात्मा रूपी पक्षी संसारिक भोग इच्छा के कारण कैद हो गया है, हमने अपने वास्तविक स्वरूप की उपेक्षा करके पिन्जरे को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लिया है, हमने अपनी सारी शक्ति इस भौतिक पिंजरे को ही संवारने में लगा रखी है, इस पिंजरे के अन्दर बन्द आत्मा की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर रखी है, यह पिंजरा-रूपी शरीर, आत्मा-रूपी पक्षी की मुक्ति के लिये प्राप्त हुआ है न कि पिंजरे की देख-भाल के लिए प्राप्त हुआ है।
यदि हम अपना ध्यान इस शरीर पर स्थिर करके यह अनुभव करें कि यह शरीर हमारी वास्तविक पहचान है अथवा नहीं, तब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि "हम इस शरीर को जानने वाले हैं, हम शरीर नहीं हैं।"
इस प्रकार की बुद्धि एक बच्चे को भी होती है, यदि हम बच्चे को उसकी अंगुली पकड़कर पूँछें, "यह क्या है?" तो बच्चे का उत्तर होगा "यह मेरी अंगुली है।" बच्चा यह कभी नही कहेगा कि "मैं अंगुली हूँ", इस शरीर का प्रत्येक अंग मेरा है परन्तु "मैं कहाँ हूँ? यही जिज्ञासा होनी चाहिये।
जहाँ वाणी की पहुँच नही होती है, मन जिसे प्राप्त नहीं कर पाता है, बुद्धि वहाँ पहुँच नही पाती है, ऐसे आत्म-स्वरूप का जो भाग्यशाली मनुष्य साक्षात्कार कर लेता है वह फिर किसी भी सांसारिक वस्तु से भयभीत नहीं होता है, मृत्यु भी उसका कुछ नही बिगाड़ पाती है, मृत्यु शरीर की होती है, आत्म-ज्ञानी उस मृत्यु का भी साक्षात्कार करता है।
"जब तक बुद्धि द्वारा मन शरीर में स्थित रहता है तब तक जीव अज्ञानी ही बना रहता है और जब बुद्धि द्वारा मन आत्मा में स्थित होने लगता है तब जीव का अज्ञान धीरे-धीरे दूर होने लगता है।"
॥ हरि: ॐ तत् सत् ॥